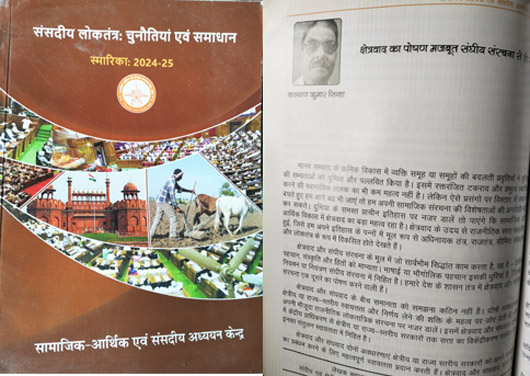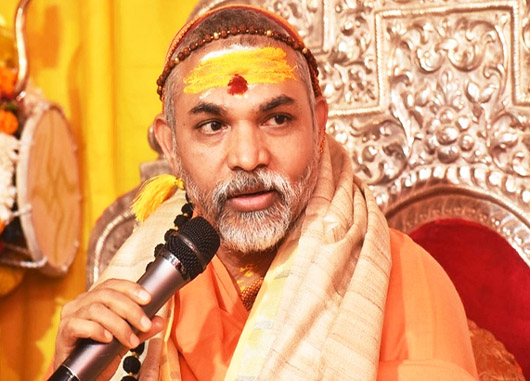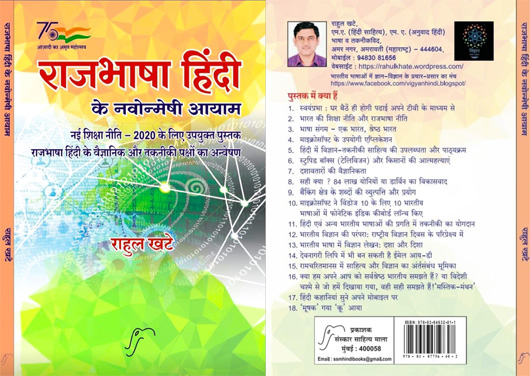सामाजिक-आर्थिक एवं संसदीय अध्ययन केंद्र, रांची की स्मरणिका 2024-25 “संसदीय लोकतंत्र : चुनौतियां एवं समाधान में प्रकाशित”
*कल्याण कुमार सिन्हा –
लेख : मानव सभ्यता के क्रमिक विकास में व्यक्ति समूह या समूहों के बदलती प्रवृतियों ने दुनिया की सभ्यताओं को पुष्पित और पल्लवित किया है. इसमें रक्तरंजित टकराव और प्रभुत्व स्थापित करने की स्वाभाविक ललक का भी कम महत्व नहीं है. लेकिन ऐसे प्रसंगों पर विस्तार से बचते हुए हम आगे बढ़ भी जाएं तो हम हमारी सामाजिक संरचना की विशेषताओं की अनदेखी नहीं कर सकते. दुनिया के समस्त प्राचीन इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि सामाजिक और आर्थिक विकास में क्षेत्रवाद का बड़ा महत्व रहा है.
क्षेत्रवाद के उदय से राजनीतिक सत्ता पल्लवित हुई, जिसे हम अपने इतिहास के पन्नों में मूल रूप से अधिनायक तंत्र, राजतंत्र, सीमित लोकतंत्र और लोकतंत्र के रूप में विकसित होते देखते हैं. क्षेत्रवाद और संघीय संरचना के मूल में जो सार्वभौम सिद्धांत काम करता है, वह है – क्षेत्रीय पहचान, संस्कृति और हितों को मान्यता. सांस्कृतिक, भाषाई या भौगोलिक पहचान इसकी धूरियां हैं, जिसका नियमन या नियंत्रण संघीय संरचना में निहित है. हमारे देश के शासन तंत्र में क्षेत्रवाद और संघीय संरचना एक दूसरे पोषण करने वाली है. क्षेत्रवाद और संघवाद के बीच समानता को समझना कठिन भी नहीं है. दोनों अवधारणाएं क्षेत्रीय या राज्य-स्तरीय स्वायत्तता और निर्णय लेने की शक्ति के महत्व पर जोर देती हैं. हम अपनी मौजूदा राजनीतिक लोकतांत्रिक संरचना पर नजर डालें. इसमें विकेंद्रीकरण: क्षेत्रवाद और संघवाद दोनों में केंद्रीय प्राधिकरण से क्षेत्रीय या राज्य-स्तरीय सरकारों तक सत्ता का विकेंद्रीकरण शामिल है. इनका संतुलन स्वायत्तता में निहित है.
क्षेत्रवाद और संघवाद दोनों अवधारणाएं क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय सरकारों को अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान करती हैं. क्षेत्रवाद और संघवाद दोनों ही क्षेत्रीय पहचान, सनातन संस्कृति और हितों को मान्यता देते हैं और उनका सम्मान करते हैं. दोनों प्रणालियों में, शक्ति केंद्र सरकार और क्षेत्रीय या राज्य-स्तरीय सरकारों के बीच साझा की जाती है.इसके अलावा, संघवाद की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जैसे- सत्ता का विभाजन, संवैधानिक सर्वोच्चता, लिखित संविधान, कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका. भारत की यही संघीय संरचना भी है. इसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने केंद्र की संघीय सरकार और राज्यों की सरकारों के लिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया है, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक जरूरतों के अनुसार विधान कर सकती हैं.
लेकिन हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि दोनों प्रणालियों में एक अंतर भी है. यह अंतर भले ही बारीक सा हो, लेकिन यह नजर आता है. क्षेत्रवाद अकसर सांस्कृतिक, भाषाई या भौगोलिक पहचान पर केंद्रित होता है. जबकि संघवाद एक व्यापक राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना है. संघवाद में, केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों की शक्तियां और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से परिभाषित होती हैं, जबकि क्षेत्रवाद में, शक्ति गतिशीलता अधिक अनौपचारिक या अस्थिर हो सकती है. संघवाद में आमतौर पर एक सुपरिभाषित संस्थागत ढांचा शामिल होता है, जैसे कि संघीय संविधान, जबकि क्षेत्रवाद में औपचारिक संस्थागत संरचना नहीं हो सकती है.
क्षेत्रवाद और संघवाद अलग-अलग अवधारणाएं हैं, जिनका शासन और राजनीतिक संगठन पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है.इन दोनों प्रणालियों के अंतर और समानता की सुंदरता को बड़ी आसानी से विद्रूप भी किए जाने के प्रयास होते रहे हैं. इसीलिए हमारे देश की संघीय संरचना को मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया जाता रहा है. अंग्रेजी शासन की गुलामी से मिली आजादी के साथ देश को विभाजन का भी गहरा दंश मिला. इसके साथ ही देश भर की देशी रियासतों, रजवाड़ों और कबीलाई समूहों को भारतीय संघ में जोड़ने या उन्हें शामिल कराने के लिए तत्कालीन भारतीय संघ की नई सरकार को भारी मशक्क्त करनी पड़ी. सरकार को क्षेत्रवाद, भाषावाद, मुस्लिम बहुल क्षेत्रवाद, हिन्दू बहुल क्षेत्रवाद, राजशाही, निजामशाही जैसे अनेक अवरोधों से गुजरना पड़ा.
इन अवरोधों पर पार पाने के बाद भी अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे देश के प्रशासनिक और क्षेत्रीय ढांचे में कई बदलाव लाए गए. राज्यों का पुनर्गठन किया गया. यह पुनर्गठन सांस्कृतिक, भाषाई या भौगोलिक पहचान पर केंद्रित रहा है. राज्यों में अभी भी उठने वाली क्षेत्रीय मांग इन्हीं भाषाई और भौगोलिक आधार पर जारी है. इस मामले में हमें बार-बार अपने संविधान निर्माताओं का शुक्रगुजार रहना पड़ेगा, जिन्होंने संविधान में देश की संघीय संरचना को इतना सुदृढ़ बनाया है कि हमारी संघ सरकार क्षेत्रवाद के उन्माद को शांत करने में भी सक्षम है, अलगाववाद को भी कुचलने में समर्थ है.
लेकिन क्षेत्रवाद और अलगाववाद की प्रवृत्तियों को राजनीतिक रूप से समर्थन दिया जाना, देश की संघीय संरचना को कमजोर करने के प्रयास के रूप में सामने आता रहा है. यह कथन कि भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि “राज्यों का संघ” है, एक राजनीतिक दृष्टिकोण है. इसके पीछे तर्क है कि भारत कई अलग-अलग भाषाओं, संस्कृतियों और पहचानों वाला देश है. लेकिन इस आधार पर उन दुष्प्रवृत्तियों को अपने राजनीतिक लाभ के लिए समर्थन दिया जाना स्वीकार्य तो नहीं हो सकता. जिसके पीछे की मंशा राजनीतिक सत्ता हथियाना हो.
यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक एकीकृत राष्ट्रीय पहचान के बजाय एक साझा इतिहास, भूगोल और राजनीतिक व्यवस्था द्वारा एक साथ बंधा हुआ देश है. जिसकी क्षेत्रीय सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना तमाम विविधताओं को एक सूत्र में पिरोई हुई है. इस सूत्र को ढीला करने अथवा कमजोर करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती. भारत का इतिहास, इसकी साझा सांस्कृतिक विरासत का इतिहास है, जो भारत की अस्मिता और मूल प्रकृति है. लेकिन यह भी सच है कि एक राष्ट्र-राज्य के रूप में भारत की अवधारणा अपेक्षाकृत आधुनिक है. जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और 1950 में भारतीय गणराज्य के निर्माण से जुड़ी है. उससे पहले, भारतीय उपमहाद्वीप कई अलग-अलग राज्यों, साम्राज्यों और औपनिवेशिक क्षेत्रों का घर था, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं. लेकिन धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक पक्ष से आपस में जुड़ी चली आईं.
इसकी अनदेखी करना एक आत्मघाती कदम साबित हो सकता है.राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भारत की विविधता को पहचानने और उसका सम्मान करने के बजाय इसके महत्व को कम करने का प्रयास, देश की संघीय संरचना को कमजोर करने की चेष्टा ही मानी जाएगी. आज की परिस्थिति में केंद्रीकृत और समरूप शासन के स्वरूप को अधिक संघीय और समावेशी दृष्टिकोण से बढ़ावा देना और देश के संविधान का सम्मान जरूरी है.
भारतीय संविधान, देश के 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करता है. भारतीय संघीय व्यवस्था के तहत, भारत का राष्ट्रपति कार्यकारी संघ का नेता होता है. दूसरी ओर, राज्य का मुखिया, जो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है. यह सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है. साथ ही संविधान में निहित संघीय संरचना क्षेत्रवाद की भावना का पोषक भी है. जो हर हाल में क्षेत्रीय भाषा, संस्कृति, आस्था, विश्वास और पहचान को बनाए रखने की गारंटी भी है.
इसके लिए देश की जनता को संविधान ने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी भी दी है. उसे सतर्क और सजग रहना होगा. अन्यथा, क्षेत्रवाद की ऐसी ओछी प्रवृत्तियों पर लगाम लगाने में 70 साल लग जाते हैं. आजादी मिलते ही केवल क्षेत्रवाद की तुष्टिकरण के लिए जम्मू-कश्मीर को संविधान में धारा 370 का प्रावधान किया जाना कितना भयावह था, आज की हमारी पीढ़ी ने प्रत्यक्ष देखा है. जिस शांति और सद्भाव के लिए देश की संप्रभुता के साथ क्षेत्रवाद के गंदे स्वरूप से समझौता किया गया था, उसका परिणाम क्या निकला? जम्मू-कश्मीर में 70 वर्षों तक अलगाववाद और दहशतवाद का तांडव चलता रहा और देश हतबल बना रहा.
क्षेत्रवाद की ऐसी ही गंदी राजनीतिक सोच का शिकार हमारा पंजाब राज्य भी हुआ. जहां अपनी राजनीतिक सत्ता बनाए रखने के लिए खालिस्तान जैसे अपवित्र मांग को परवान चढ़ा दिया गया. बाद में उसी खालिस्तानी सोच को कुचलने और अमृतसर के पवित्र हरमंदिर साहिब को खालिस्तानी उग्रवादियों से मुक्त कराने के लिए सेना को आगे लाना पड़ा. इतना ही नहीं, उसी के बदले की आग में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं खालिस्तानी सोच ने गोलियों का शिकार बना दिया. जिसे इंदिरा गांधी ने बढ़ावा दिया था. गंदे और स्वार्थ के क्षेत्रवाद ने फिर से सर उठा कर केवल पंजाब में ही नहीं, पूरे देश में कठिन परिस्थिति पैदा कर रहा है.
पूर्वी राज्यों की विविधतापूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान का सम्मान शांति और सद्भाव के लिए कितना जरूरी है, यह पूरा देश महसूस करता है. इन राज्यों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आजादी के 60-70 सालों तक नहीं के बराबर प्रयास हुए. लेकिन जब उन्हें मुख्य धारा के साथ मजबूती के साथ जोड़ने के प्रयास फलीभूत होने लगे हैं, वहां फिर से अशांति और जातीय भेदभाव फैलाने की कोशिशें जारी हैं. ऐसी परिस्थिति में इन राज्यों में भी देश की संघीय संरचना की मजबूती ही काम आ रही है.
इन दुखद प्रसंगों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए संविधान में किया गया धारा 6 के प्रावधान की भी चर्चा जरूरी है. जिसके तहत असम पर अपनी राजनीतिक सत्ता की पकड़ बनाए रखने के लिए 1970 तक बांग्लादेश से असम में घुस आए लोगों को भारत नागरिक मान लेने का प्रावधान कर दिया गया. इस धारा 6 का परिणाम यह है कि असम में घुसपैठ बढ़ता गया और आज वहां के स्थानीय आबादी अल्पसंख्यक होने की कगार पर पहुंच गई है.
देश में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हालांकि क्षेत्रीय पहचान, संस्कृति और हितों को मान्यता. सांस्कृतिक, भाषाई या भौगोलिक पहचान के आधार पर ही हुआ है. लेकिन इसके पीछे देश की संघ सरकार पर आरंभ से ही अंग्रेजों की विरासत संभालने वाली कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका रही. अंग्रेजों की देश की सत्ता हासिल करने का उद्देश्य केवल अपना व्यापारिक स्वार्थ रहा. शासन तंत्र को भी उसने उसी हिसाब से विकसित किया. उनके शासन तंत्र में जनता के हितों का स्थान बहुत ही सीमित था. विरासत में कांग्रेस को जब सत्ता मिली तब उसने समाजवाद का ढोंग तो रचा, लेकिन देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय विविधता को नजरअंदाज ही किया.
आज जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी है, वह क्षेत्रीय दलों का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए ही कर रही है. अपनी तुष्टिकरण की नीति के आधार पर जातीय विभेद को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रवाद की मूल जनहितकारी भावना को छिन्न-भिन्न करने पर तुली हुई नजर आ रही है. संघीय सरकार, चाहे वह केंद्र की हो या राज्यों की, उनके प्रति जनमानस में भ्रम फैलाने की राजनीति पर उतर आई है.
ऐसे में क्षेत्रवाद और हमारी संघीय संरचना को अक्षुण्ण बनाए रखने और इनका जतन करना जरूरी है. क्षेत्रवाद की मूल अवधारणा को दूषित होने से बचाना होगा. साथ ही अपने देश की संघीय संरचना को भी मजबूती देने के लिए राष्ट्रवादी सोच को सत्ता में बनाए रखने के हर संभव उपाय अपनाने होंगे.

– कल्याण कुमार सिन्हा (वरिष्ठ पत्रकार).